: सभ्यता कितनी भी सभ्य हो जाये, अपनी मर्द होने की मर्दानगी से समझौता नहीं करती : यवनों ने हमारे रंगमंच और रंगकर्म को समृद्ध किया : दूसरी संस्कृतियां हमें सिखा रही हैं, हम विश्वगुरु होने का दर्प पाले बैठे हैं :
कुमार सौवीर
 लखनऊ : करीब चालीस बरस पहले मैंने पढ़ी थी महापण्डित राहुल की महान रचना, जिसने जीवन और समाज के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया था। किताब का नाम है “वोल्गा से गंगा”। आज जगदीशपुर वाले पाण्डेय खानदान के शिवम, रजनी और रंजीत के घर यह किताब फिर दिख गयी। शिवम और रंजीत उसे पहले ही पढ़ चुके थे, रजनी किताब के कथ्य वाले मर्म खोजने में जुटी थीं।
लखनऊ : करीब चालीस बरस पहले मैंने पढ़ी थी महापण्डित राहुल की महान रचना, जिसने जीवन और समाज के प्रति मेरा नजरिया ही बदल दिया था। किताब का नाम है “वोल्गा से गंगा”। आज जगदीशपुर वाले पाण्डेय खानदान के शिवम, रजनी और रंजीत के घर यह किताब फिर दिख गयी। शिवम और रंजीत उसे पहले ही पढ़ चुके थे, रजनी किताब के कथ्य वाले मर्म खोजने में जुटी थीं।
बस यूं ही, मैंने इस महान कृति के पन्ने पलटते वक्त साकेत के कुछ नवोदित युवक-युवतियों का किस्सा पढ़ने लगा, जिसमें एक समारोह से निकल रहे महानतम महामानव अश्वघोष को साकेत रंगकर्मियों ने टोक कर उनसे बातचीत शुरू की थी। उन रंगकर्मियों ने अश्वघोष से यह भी आग्रह किया कि वे भी साकेत में बसे कुछ यवन-यवनियों के साथ उनके रंग-प्रेक्षागृह में आ कर उन्हें अनुग्रह करें। यह लंबी चर्चा है, जिस पर अलग से विस्तृत बातचीत हुई ही चाहिए।
लेकिन इस वक्त अब यह बात इस या किसी दीगर किताब से अलग। तनिक सोचिए कि आज तो हम अपने धर्म और समाज के विभिन्न जातियों के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जातीयता को लेकर घटिया और हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उस वक्त का समाज सात समंदर पार वाले देश से आये यवनों से न सिर्फ तादात्म्य कर कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी स्थापित कर उसे और अश्वघोष जैसी महानतम विभूतियों के साथ जोड़ने का अभियान भी छेड़े हैं।
तो, अब बताइये कि घृणित कौन ?
महोदय ! संस्कृति वह नहीं होती, जिसे आप अपने जंगल से जकड़ कर उसे बाकी सभ्यता से दूर रखने की भरसक कोशिश करते हैं। बल्कि संस्कृति तो एक निर्मल झरने-सरिता की तरह कलकल बहती ही रहती है। उसके प्रवाह को रोकना भयावह अनिष्ट को पसार देना ही तो है।
खैर, लेकिन इससे पहले तो एक सवाल और तैर रहा है कि किसी भी कला में “यवनिका-पतन” ही क्यों होता है।
सभ्यता कितनी भी सभ्य हो जाये, अपनी मर्द होने की मर्दानगी से समझौता नहीं करती है।
क्यों ?
क्या मैं गलत पूछ्या ?
( यह किताब महल की प्रस्तुति है। अनावश्यक मोटे हर्फ़ों में है, शायद मोटा साबित करने की साजिश के तहत, ताकि उसका कथ्य भी ज्यादा मोटा दिखे। बकवास। कीमत भी बेहिसाब। मेरी हैसियत होती तो मैं यही किताब एक सौ रुपल्ली में ही छपवा देता ? लेकिन हिंदी के पाठक ही घटिया, निर्लज्ज, पापी, स्वार्थी और आत्मघाती होते जा रहे हैं, तो क्या किया जाए।)


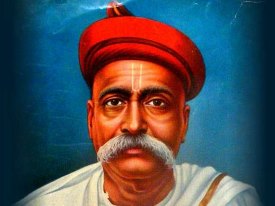
🙏🙏🙏🙏🙏